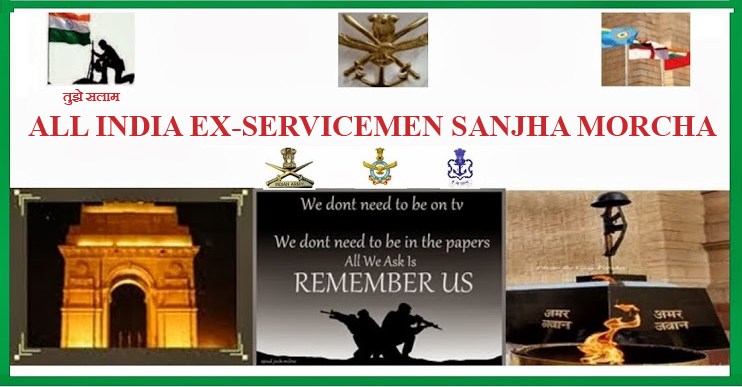भारत जैसा देश जिसके पास समुद्री तटों पर रहने वाली आबादी हो तो यह लाजिमी हो जाता है कि वह उसकी समुद्रवर्ती सुरक्षा का ध्यान रखे। चीन और पाकिस्तान से लगने वाली अपनी समुद्री और जमीनी सीमाओं की सुरक्षा संबंधी दरकारों ने भारत के लिए इस जरूरत को ज्यादा उभार दिया है। आजादी के बाद कई दशकों तक आयात के विकल्प ढूंढने की नीति के चलते विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा बहुत कम रह गया था। 1990 में आर्थिक चुनौती के बाद भारत को अपनी आर्थिक नीतियों में भारी फेरबदल करने पर मजबूर होना पड़ा था। इसके बाद हुआ यह कि भारत की अर्थव्यवस्था का एकीकरण न सिर्फ वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ हुआ बल्कि एक बढ़ते बाजार की बदौलत व्यापार और निवेश के लिए मुफीद माने जाने से हमारा देश वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक रचनात्मक और सतत महत्वपूर्ण सदस्य बनकर भी उभरा। तब से लेकर हम उस जीर्ण अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़कर एक गतिशील और उभरती हुई आर्थिक शक्ति में परिवर्तित हो चुके हैं।
भारत जैसा देश जिसके पास समुद्री तटों पर रहने वाली आबादी हो तो यह लाजिमी हो जाता है कि वह उसकी समुद्रवर्ती सुरक्षा का ध्यान रखे। चीन और पाकिस्तान से लगने वाली अपनी समुद्री और जमीनी सीमाओं की सुरक्षा संबंधी दरकारों ने भारत के लिए इस जरूरत को ज्यादा उभार दिया है। आजादी के बाद कई दशकों तक आयात के विकल्प ढूंढने की नीति के चलते विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा बहुत कम रह गया था। 1990 में आर्थिक चुनौती के बाद भारत को अपनी आर्थिक नीतियों में भारी फेरबदल करने पर मजबूर होना पड़ा था। इसके बाद हुआ यह कि भारत की अर्थव्यवस्था का एकीकरण न सिर्फ वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ हुआ बल्कि एक बढ़ते बाजार की बदौलत व्यापार और निवेश के लिए मुफीद माने जाने से हमारा देश वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक रचनात्मक और सतत महत्वपूर्ण सदस्य बनकर भी उभरा। तब से लेकर हम उस जीर्ण अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़कर एक गतिशील और उभरती हुई आर्थिक शक्ति में परिवर्तित हो चुके हैं।
विदेश व्यापार और निवेश भारत की तेजी से बढ़ती हुई आर्थिक वृद्धि के अनिवार्य केंद्र बिंदु बन गए हैं। हमने अपनी आर्थिकी को पूर्व और दक्षिण-पूर्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं से जोड़कर समझदारी वाला काम किया है। आसियान’ संगठन के 10 देश जिनमें म्यांमार से लेकर फिलीपींस और जापान और दक्षिण कोरिया इत्यादि भी हैं, उनके साथ अब हमारी बृहद आर्थिक साझेदारी है। इसके अलावा हम आस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार संधि’ करने के लिए बातचीत कर रहे हैं और अन्य दक्षेस देशों के साथ भी इसी तरह के समझौते करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे भी ज्यादा यह कि आसियान’ के नेतृत्व वाले मंच जैसे कि पूर्वी एशिया शीर्ष वार्ता’ ने भारत को बंगाल की खाड़ी में बड़ी सामरिक भूमिका निभाने का मौका प्रदान किया है। हालांकि दक्षिण एशिया के देशों के बीच एकीकृत आर्थिक व्यवस्था बनाने की गति धीमी रही है, इसका मुख्य कारण पाकिस्तान का अडि़यल रवैया रहा है। महत्वपूर्ण यह है कि विश्व के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले दो देशों, चीन और भारत के बीच कुछ तनाव और विवाद वाले मुद्दे भी आपसी व्यापार और निवेश के माहौल को फलने-फूलने से नहीं रोक पाए।
भारत इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि जब भी हमारे देश ने अपनी पूर्वी सीमा के पार अपनी भूमिका को बढ़ाने का प्रयास किया है तब-तब चीन ने हर उस काम में रोड़ा अटकाने का काम किया है। मसलन बीजिंग की सरकार ने भारत द्वारा पूर्वी देशों की विभिन्न समितियां जैसे कि आसियान’ संगठन, आसियान क्षेत्रीय मंच’ और पूर्वी एशिया शीर्ष वार्ता’ के साथ अपने आर्थिक और सुरक्षा संबंधी रिश्ते बनाने के प्रयासों की कड़ी मुखालफत की है। वहीं दूसरी ओर चीन म्यांमार की सीमा के अंदर से भारत के खिलाफ मुहिम चलाने वाले उत्तर-पूर्वी पृथकतावादी संगठनों के साथ अपने संबंध बनाए हुए है। परंतु अब हम ऐसे चीनी प्रयासों का प्रत्युत्तर देने के लिए लगातार सार्थक सक्रियता बढ़ाने की ओर अग्रसर हैं। हमारा ध्येय अपनी पूर्वी सीमा से लगे देशों के साथ एक व्यावहारिक सुरक्षा तंत्र विकसित करने का है। बंगाल की खाड़ी के इलाके में अपने सैन्य अड्डे और पैठ बनाने के चीनी प्रयासों की वजह से हमारी चिंता बनी रहेगी। लेकिन अपने सहयोगी देशों जैसे कि अमेरिका और जापान के साथ बने सहमतिपूर्ण राजनयिक प्रयासों ने भारत को यह मौका प्रदान किया है कि वह अपनी पूर्वी सीमा के समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर सके। म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव में अपनी प्रधान भूमिका तय करवाने में चीन सफल नहीं हो सका है। जहां एक ओर भारत ने अपने पूर्वी तटों पर सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अपनी नीतियों में परिवर्तन किया है, वहीं दूसरी ओर पश्चिम में स्थित अरब सागर के इर्द-गिर्द वाले हमारे पड़ोसी देशों के बीच क्या पक रहा है, यह ठीक से कहा नहीं जा सकता। चीन न केवल हिंद महासागर में स्थायी सैन्य उपस्थिति बनाने की ओर अग्रसर है बल्कि ऐसा वह पाक के साथ मिलकर कर रहा है। भारत को चीन के इस किस्म के प्रयासों का संज्ञान लेते हुए उन परियोजनाओं पर पैनी नजर रखनी होगी, जिनके तहत वह हमारी पश्चिमी सीमा के पार वाले इलाके में सड़कों और बंदरगाहों का नेटवर्क बनाकर बढ़त बनाने की कोशिश में है। चीन अपने सामरिक उद्देश्य की पूर्ति की खातिर एक सिल्क रोड आर्थिक पट्टी’ बनाने जा रहा है जो उसे मध्य-एशिया, पाक-अधिकृत कश्मीर, फारस की खाड़ी, रूस और बाल्टिक देशों से जोड़ देगी। इसके अलावा चीन 21वीं सदी का एक ऐसा समुद्री-सिल्क-मार्ग भी बनाने जा रहा है जो उसके तटों से शुरू होकर हिंद महासागर से होता हुआ पश्चिमी देशों तक जाएगा। साथ ही चीन हिंद महासागर, एशिया और अफ्रीकी देशों में बंदरगाह बना रहा है। जिस बात से भारत के लिए आंखें मूंदना ठीक नहीं होगा, वह है कि सिल्क रोड’ हमारे पूर्वी और पश्चिमी, दोनों पड़ोसियों को अपने पाश में लेती हुई बनेगी और यही सड़क समुद्री-सिल्क-मार्ग’ की राह में पड़ने वाले हिंद महासागर के तटों और अरब सागर के मुहाने पर स्थित पाकिस्तान के गवादर बंदरगाह तक संपर्क बनाने का काम भी करेगी।
चिंता की बात यह है कि भारत के समुद्री-मार्ग गवादर के काफी पास से होकर गुजरते हैं और इनके जरिए फारस की खाड़ी में स्थित देशों से हमारा 70 फीसदी से ज्यादा कच्चा तेल आयात किया जाता है। अब चीन ने अपनी इन महत्वाकांक्षी जमीनी और समुद्री सिल्क रोड परियोजनाओं को बढ़ावा देने के एवज में पाकिस्तान को 46 बिलियन डॉलर देने का वादा किया है ताकि वह इसके गवादर बंदरगाह का लाभ उठाते हुए नियंत्रण एक तरह से अपने हाथों में कर सके। कोई एक दशक पहले तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने इस्लामाबाद में कहा था कि भारत-पाक युद्ध होने की सूरत में भारत यह पाएगा कि चीनी नौसेना हमारी मदद को गवादर बंदरगाह में तैनात है। चीन को लगता है कि पाकिस्तान एक बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी इसलिए भी है क्योंकि गवादर न सिर्फ होरमुज जलडमरू के पास स्थित है बल्कि इसके पास होकर भारत के समुद्री जहाज खाड़ी के उन देशों तक जाते हैं, जहां पर लगभग उसके 7 लाख प्रवासी कामगार हैं।
चीन की अत्यधिक रुचि का इस तथ्य से पता चलता है कि यह दो मील चौड़ा समुद्री-गलियारा वह है, जिसके माध्यम से 1.7 करोड़ बैरल कच्चा तेल रोजाना ढोया जाता है। जलमार्ग आगे चलकर मालाका जलडमरू से होकर गुजरता है। इस समुद्री रास्ते के जरिए 1.42 करोड़ बैरल कच्चा तेल जापान को जाता है। यह मात्रा उसके कुल तेल आयात की 80 फीसदी बनती है। समूचा हिंद महासागर क्षेत्र जो अदन की खाड़ी तक फैला है, पूरे संसार के कुल तेल उत्पादन का 40 फीसदी और विश्व तेल व्यापार में 57 फीसदी हिस्सा रखता है। इसीलिए अमेरिका ने इन अति-महत्वपूर्ण सामरिक नौवहनीय मार्गों की सुरक्षा की खातिर बहरीन स्थित नौसैनिक अड्डे में अपना पांचवां बेड़ा तैनात कर रखा है।
आदर्श स्थिति तब होगी जब एशिया के मुख्य तेल आयातक देश जैसे कि भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया उन परिस्थितियों पर आपसी सहयोग बनाएं जिनकी वजह से इन महत्वपूर्ण तेल और ऊर्जा सप्लाई समुद्री मार्गों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। लेकिन मौजूदा तनाव और आपसी शक के चलते ऐसा होने की उम्मीद करना ज्यादा ही अपेक्षा करने जैसा होगा, कम से कम निकट भविष्य में इसकी संभावना नहीं है।